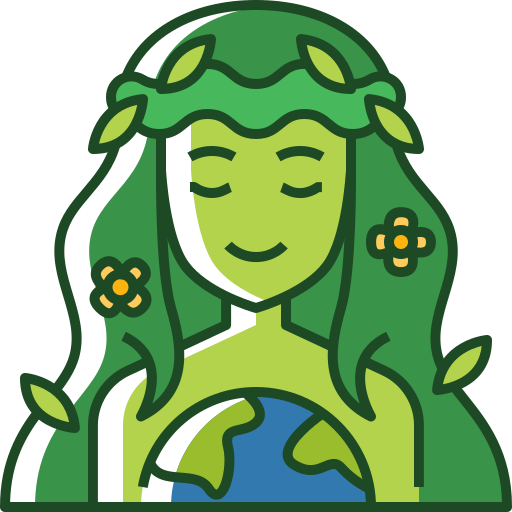नवरात्रि और नौ औषधीय पौधों के बीच पवित्र संबंध: एक पारंपरिक और चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य
गुड़ी पड़वा अर्थात चैत्र नवरात्रका प्रारम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को होने के साथ ही विक्रम संवत् जो पंचांग राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से ही जारी, का भी प्रारंभ होता हैएवं दक्षिण भारत में इसे उगादी कहा जाता है। नवरात्रि, एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है, जिसे हिन्दू नववर्ष उत्सव के रूप में भी पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा के नौ रूपों के लिए उपवास, अनुष्ठान और प्रार्थनाएँ की जाती हैं। जिन्हें सामूहिक रूप से नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग नवीन वस्त्र पहनते हैं, घरों की साफ़ सफाई कर उसे सुसज्जित करते हैं, आम्रपत्र लरी सेनिर्मित बंदनवार से द्वार सजा कर रंगोली बनाते हैं। यद्यपि वर्ष भर मेंशारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों ही देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं, लेकिन वे समय और महत्व के मामले में भिन्न हैं। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जबकि शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में आती है और आगामी फसल के मौसम का प्रतीक है। भाव भक्ति के साथ साथ इस त्यौहार का सम्बन्ध प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। तभी तो फाल्गुन मास के वासंती बहार के इस माह में प्रकृति में चारों ओर उत्साह और सौंदर्य व्याप्त है तथ बसंत ऋतु के आगमन के लिए संपूर्ण प्रकृति नव वर्ष के स्वागत करने को आतुर प्रतीत होती है। जिसमें खेतों में पुष्पित सरसों के पीले-पीले पुष्प और गेहूं की झूमती हुई बालियां, निर्जर सघन वनों में खिले रक्तवर्णी पलाश और सेमल के फूलों का अनुपम सिन्दूरी सौंदर्य मिलकर प्रकृति के सुंदरता का वास्तव में उत्सव मना रहे होते हैं। मंजरियों से लदे आम्र के वृक्ष, नयी कोपलें, कोयल की मधुर कूक, भौंरों को आकर्षित करने लगती है. चारों ओर प्रकृति का ही उत्सव चल रहा होता है और इस मधुमासीय रंगोत्सव के साथ नव संवत्सर का आगमन होता है चैत्र नवरात्र के रूप में। जिसका प्रत्येक दिवस देवी केअलग-अलग रूप को समर्पित होता है-
प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ।।
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च।
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ।।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः।
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना।
(दुर्गासप्तशती-श्रीचण्डीकवच 3-5)
अर्थात् देवी की नौ मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, द्वितीयब्रह्मचारिणी तथा तृतीय स्वरूप चन्द्रघण्टा के नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्थ स्वरूप को कूष्माडा, पञ्चम स्वरूप स्कन्दमाता, षष्टम स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। सप्तम स्वरूप कालरात्री और अष्टम स्वरूप महागौरी के नाम से प्रिसद्ध है। नवम स्वरूप को सिद्धिदात्री कहते हैं। ये स नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान् के द्वारा ही प्रितपादित हुए हैं।
प्रत्येक दिवस एक विशिष्ट पौधे से जुड़ा होता है जो दिव्य ऊर्जा, पवित्रता और स्वास्थ्य लाभ का प्रतीक होता है। इस लेख के माध्यम से नवरात्रि के प्रत्येक नवदुर्गा स्वरूप के साथ इन पौधों के संबंध की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है, जो आध्यात्मिकता और प्रकृति के बीच सहजीवी संबंध को उजागर करता है। इन पादपों अथवा वनस्पतियों को पारंपरिक चिकित्स्कीय ज्ञान के आधार पर उनके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अतः इन पवित्र पौधों को दैनिक जीवन में प्रयोग करने से समग्र कल्याण में योगदान मिल सकता है।
1. प्रथम नवदुर्गारूप:

शैलपुत्री शैलपुत्री (शैलपुत्री), पर्वत राजा हिमवत की पुत्री हैं, और हिंदू देवी माँ दुर्गा का एक रूप है। शैलपुत्री दो शब्दों शैल तथा पुत्री से मिलकर बना है। शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ पुत्री है। इसलिए पर्वत की पुत्री का सार एक आवश्यक जड़ी बूटी में समाहित है जिसे हरीतकी या (टर्मिनलिया चेबुला) के नाम से जाना जाता है।
- सम्बंधित पादपः हरड़ / हरीतकी
- वैदिक नामःवीरकः हरीतकः
- वानस्पतिक नाम: Terminalia chebula.
- संस्कृत नामः हरीतकी को संस्कृत में भया, अव्यथा, पथ्या, कायस्था, पूतना, हरीतकी, हैमवती, चेतकी, श्रेयसी, शिवा आदि नामों से जाना जाता है।
चिकित्सीय उपयोगः
हरीतकीमधुर, तिक्त, कषाय होने से पित्त; कटु, तिक्त, कषाय होने से कफ तथा अम्ल, मधुर होने से वात का शमन करती है। इस प्रकार यह त्रिदोष हर है। प्रभाव से यह वात प्रकोप नहीं करती, इसलिए त्रिदोष हर है। यह रूखी, गर्म, जठराग्नि वर्धक, बुद्धि को बढ़ाने वाली, नेत्रों के लिए लाभकारी, आयुवर्धक, शरीर को बल देने वाली तथा वात का शमन करने वाली है। यह श्वास, कास, प्रमेह, बवासीर (अर्थ), कुष्ठ, सूजन, उदर-रोग, कृमि रोग, स्वर भंग, ग्रहणी, विबंध, गुल्म, आध्मान, व्रण, थकान, हिचकी, कंठ और हृदय के रोग, कामला, शूल, अनाह, प्लीहा व यकृत के रोग, पथरी, मूत्र कृच्छ्र और मूत्र घातादि रोगों को दूर करती है। हरड़ का फल व्रण के लिए हितकारी, उष्ण, सर, मेध्य, दोषनाशक, शोथ, कुष्ठनाशक, कषाय, अग्निदीपन, अम्ल तथा आंखों के लिए हितकारी है। हरड़ में पांचों रस साथ रहकर भी प्रकोप नहीं करते। इसलिए एक ही हरीतकी अनेक रोगों में प्रयोग की जाती है। हरीतकी की मज्जा में मधुररस, नाड़ियों में अम्लरस, वृन्तमें कड़वा रस, छाल में कटु रस और गुठली में कसैला रस रहता है।
विशिष्टगुणवकार्य-
चबाकर खाई हुई हरड़ अग्निवर्धक, पीसकर खाई हुई दस्तावर, उबालकर खाई हुई दस्त बन्द करती है। भूनकर खाई हुई त्रिदोष हर, भोजन के साथ खाई हुई हरड़ बुद्धिबल तथा इद्रियों को प्रसन्न करतीहै, भोजन के उपरांत खाई हुई हरीतकी मिथ्या अन्न-पान से होने वाले सब विकारों को दूर करती है। राजवल्लभ निघण्टु में हरितकी के लिये कहा है कि-यस्य माता गृहे नास्ति, तस्य माता हरीतकी। कदाचित कुप्यते माता, नदोरस्था हरीतकी।।
अर्थात् जिसके घरमें माता नहीं है, उसकी माता हरीतकी है। माता तो कभी- कभी कुपित भी हो जाती है, परन्तु सेवन की हुई हरड़ कभी भी कुपित नहीं होती। वसन्त ऋतु में शहद के साथ इसके सेवन का विधान किया गया है। यह शरीर के कोष्ठों में व्याप्त विषों को बाहर निकालने में सक्षम होती है।
2. द्वितीय नवदुर्गारूपः ब्रह्मचारिणी

ब्रह्मचारिणी भक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। यह देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम है। इस स्वरूप की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है।
- सम्बंधितपादप- ब्राह्मी
- वैदिक नाम:ब्राह्मिका मेध्या
- वानस्पतिक नाम: Bacopa monnieri (L.) Wettst.
- संस्कृत नामः ब्राह्मी को संस्कृत में कपोत वङ्का, सोमवल्ली, सरस्वती, ब्राह्मी, ऐद्री; आदि नामों से जाना जाता है।
चिकित्सीय उपयोगः
ब्राह्मी कषाय, मधुर, तिक्त, शीत, लघु कफ वात शामक, आयुवर्धक, बुद्धिवर्धक, रसायन, स्वरवर्धक, वयःस्थापक, दीपन, सर, स्मृतिवर्धक, प्रजास्थापन, कंठ शोधक तथा हृद्य होती है। यह कुष्ठ, पाण्डु, प्रमेह, शोथ, विष, ज्वर, कण्डू, प्लीहारोग, अरुचि, श्वास, कास, मोह, उन्माद, हृदय रोग तथा अग्निमांद्य, विबन्ध, दौर्बल्य एवं वात रक्त नाशक होती है। इसका पञ्चाङग प्रशामक, पेशी शैथिल्य कारक, उद्वेष्टरोधी, कर्कटार्बुद रोधी, वेदना शामक, स्तम्भक, हृदय बल कारक, मूत्रल, मस्तिष्क बल कारक, विरेचक, वातानुलोमक, पाचक, शोथरोधी, आक्षेपरोधी, शोधक, श्वसनी विस्फारक, स्वेदकारक, आर्तव वर्धक तथा ज्वरघ्न होता है। इसके लिये आयुर्वेद में कहा है-बुद्धि प्रज्ञं च मेधा च कूर्यादायुष्यवर्द्धनी (राजनिघण्टु पर्पटादिवर्ग-66) ब्राह्मी क प्रयोग विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों की चिकित्सा में किया जाता है।
3. तृतीय नवदुर्गारूपः चंद्रघंटा-

देवी के तृतीय स्वरूप को -चंद्र-घंटाके नाम से जाना जाता है। उन्हें चंद्रखंडा, चंडिका या रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रघंटा के साथ औषधीय पौधे चंद्रसूर /लेपिडियम सैटिवम को दर्शाया गया है।
- सम्बंधितपादप- चंदसूर
- वैदिक नामः चन्द्रशूरकः
- प्रायतकोशः
- वानस्पतिक नामः (Lepidium sativum L.)
संस्कृत नामः
इसे संस्कृत में चन्द्रिका, चर्महत्री, पशु मेहन कारिका, नदनी, कारवी, भद्रा, वासपुष्पा, सुवासरा, चंद्रसूरम्, चंद्रसूराआदि नामों से जाना जाता है।
चिकित्सीय उपयोगः
चंद्रशूरकटु, उष्ण, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, वात कफ शामक, बल पुष्टि वर्धक, स्तन्य वर्धक, वृष्य तथा वाजी कर होताहै। यह हिक्का, अतिसार, शूल, गुल्म, त्वचारोग, वातरोग, नेत्ररोग, कृमिरोग, अभिघात-जन्य वेदना तथा वेदना-नाशक होता है। इसका पत्र तथा प्ररोह यकृत्-विकार, शीतपित्त, हिक्का, उरः शूल, भम तथा शोथ शामक होता है। इसकी मूल कटु, तिक्त, वेदना स्थापन, जंतुघ्न, त्वग दोषहर, दीपन, वातानुलोमन, रक्तशोधक, कफनिः सारक मूत्रल, वृष्य, आर्तवजनन, वाजीकर तथा उत्तेजक होती है। इसके बीज तिक्त, शोधक, रक्तिमाकर, आर्तववर्धक, गर्भस्रावक, स्मृति वर्धक तथा मूत्रल होते हैं। इसका फल नेत्र रोग तथा त्वम्-रोग-शामक होता है। इसके बीज से निर्मित उपनाहकुष्ठ, त्वगरोग, अतिसार, प्लीहावृद्धि, अजीर्ण, कटिशूल, नेत्ररोग, श्वेत प्रदर, शीताद्, श्वासकष्ट, शुक्र-दौर्बल्य, कास, हिक्का, अर्श, आमवात तथा सूति का ज्वर-शामक होता है।
4. चतुर्थनवदुर्गारूपः कूष्मांडा-

ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली देवी कुष्मांडा, को कलिकुला परंपरा के अनुयायी उन्हें देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप मानते हैं। नाम के अनुसार कूष्मांड का सम्बंध कूष्मांडा देवी के स्वरूप से है।
- सम्बंधित पादप- पेठा
- वैदिक नामः कूष्माण्डकः कुम्भफलः
- वानस्पतिक नाम: Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
- संस्कृत नामः इसे संस्कृत में चन्द्रिका कूष्माण्डम्, पुष्पफलम्, बृहत्फलम्, वल्लीफलम्, पीतपुष्पाम्; आदि नामों से जाना जाता है।
चिकित्सीय उपयोगः
इसके फलों से निर्मित पेठा मिठाई को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। कूष्माण्ड मधुर, शीत, लघु, गुरु, स्निग्ध, वात पित्त शामक; कफ कारक, बृंहण, वृष्य, दीपन, धातुवर्धक, पुष्टिकारक, वस्तिशोधक, हृद्य, मूत्रल, बलकारक, केश्य, अभिष्यंदि तथा विष्टंभ कारक होता है। कूष्माण्ड मूत्रा घात, अश्मरी, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, तृष्णा, अरोचक, शुक्रविकार तथा रक्त विकार-नाशक होता है। बाल कूष्माण्डशीत, कफ कारक तथा पित्त शामक होताहै। कूष्माण्डकाशाक मधुर, गुरु, उष्ण, वात शामक, अग्निदीपक, रोचक, सारक, ज्वर, आमदोष, शोफतथादाह-नाशक होता है। पक्वकूष्माण्ड मधुर, अम्ल, लघु, त्रिदोषशामक, मल-मूत्र को निकालने वाला तथा शुक्र रोग-नाशक होता है। कूष्माण्ड-तैलमधुर, शीत, गुरु, वातपित्त-शामक, कफकारक, अभिष्यन्दि, विबंधहर, अग्निसादक एवं केश्य होता है। आयुर्वेदीय ग्रन्थों में कूष्माड की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि –
मूत्राघातहरं प्रमेहशमनं कृच्छ्राश्मरीच्छेदनं
विण्मूत्रग्लपनं तृषार्त्तिशमनं जीर्णाङ्गपुष्टिप्रदम् ।
वृष्यं स्वादुतरं त्वरोचकहरं बल्यं च पित्तापहम् कूष्माडं प्रवरं भिषजो वल्लीफलानां पुनः।
(राजनिघण्टु मूलकादिवर्ग-160)
गुण-
कूष्माड मूत्राघात को दूर करने वाला, प्रमेह-शामक, मूत्रकृच्छ्र तथा पथरी का छेदन करने वाला, मलमूत्र को शिथिल, तृषा को शान्त, दुर्बल अङ्गों को पुष्ट करने वाला स्वादिष्ट, अरुचिनाशक तथा पित्तनाशक होता है। वैद्यों ने लता पर लगने वाले फलों में कूष्माड को सर्वश्रेष्ठ कहा है। (राजनिघण्टु मूलकादिवर्ग-160)
5. पंचमनवदुर्गारूप: स्कंदमाता-

देवी दुर्गा का पांचवा रूप स्कंदमाता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे भगवान कार्तिकेय (स्कंद) की माता हैं, और इनसे संबंधिति औषधि के रूप में अलसी का ग्रहण किया माता हैं, और इनसे संबंधिति औषधि के रूप में अलसी का ग्रहण किया जाता है।
- सम्बंधितपादप- अलसी
- वैदिक नामः अतसिका नीलपुष्पा
- वानस्पतिक नाम: Linum usitatissimumL.
- संस्कृत नामः इसे संस्कृत में अतसी, नीलपुष्पी, नीलपुष्पिका, उमा, क्षुमा, मसरीना, पार्वती, क्षौमी; आदि नामों से जाना जाता है।
चिकित्सीय उपयोगः
अलसी के बीज मधुर, मंदगंध-युक्त, स्निग्ध, उष्ण, चरपरे, गुरु, बलकारक, कामोद्दीपक, अल्पमात्रा में मूत्रकारक, शोथहर, अधिक मात्रा में रेचक, वात शामक तथा वात रक्त, कुष्ठ, व्रण, पृष्ठशूल, शुक्र, कफ वपित्त शामक होते हैं। अलसी तेल-मधुर, पिच्छिल, वातशामक, मंदगंधि, कुछ कसैला, बलकारक, भारी, गर्म, मलकारक, स्निग्ध, ग्राही, कफ शामक, कास नाशक तथा त्वक्-दोषहर है। अलसी-पत्रकास, श्वास, कफ तथा वातशा मक, इसके ताजे हरे पत्तों की शाक वातग्रस्त रोगियों के लिए विशेष लाभदायक है। अलसी-पुष्परक्ता-पत्त-शामक होता है। भुने हुएअलसी बीज स्तम्भक तथा वेदना-शामक होते हैं।
6. षष्टः नवदुर्गारूपः कात्यायनी –

देवी कात्यायनी को कई नामों जैसे अम्बा, अम्बालिका व अम्बिका से जाना जाता है। इनसे संबंधिति औषधि के रूप में माचिका का जिसे मोइया भी कहते हैं का ग्रहण किया जाता है।
- सम्बंधितपादप- मोइया
- वैदिक नामः झाबुकः आच्छदपत्रः
- वानस्पतिक नाम: Tamarix aphylla (L.) H.Karst.
- संस्कत नामः इसे संस्कत में माचिका. सचिमखी. साकण्ठमखीः ; आदि नामों से जाना जाता है।
चिकित्सीय उपयोगः
यह कषाय, तिक्त, अम्ल, मधुर रस से युक्त वृष्य, बल्य, शूलाघ्न, अग्नि प्रदीपक, रुचि कारक तथा उष्ण होती है। इसका प्रयोग प्लीहा रोग, पक्का तिसार, कण्ठरोग, गुल्म, उदररोग, पाण्डु, आनाह, शीत ज्वर तथा रक्त पित्त नाशक की चिकित्सा में किया जाता है। माचिका को पीसकर लगाने से पामा तथा अन्य त्वचा विकारों का शमन होता है। माचिका चूर्ण से निर्मित क्वाथ का कवल धारण करने से गलशुण्डी शोथ तथा दंत शूल में लाभ होता है।
7. सप्तमः नवदुर्गारूपः कालरात्रि-
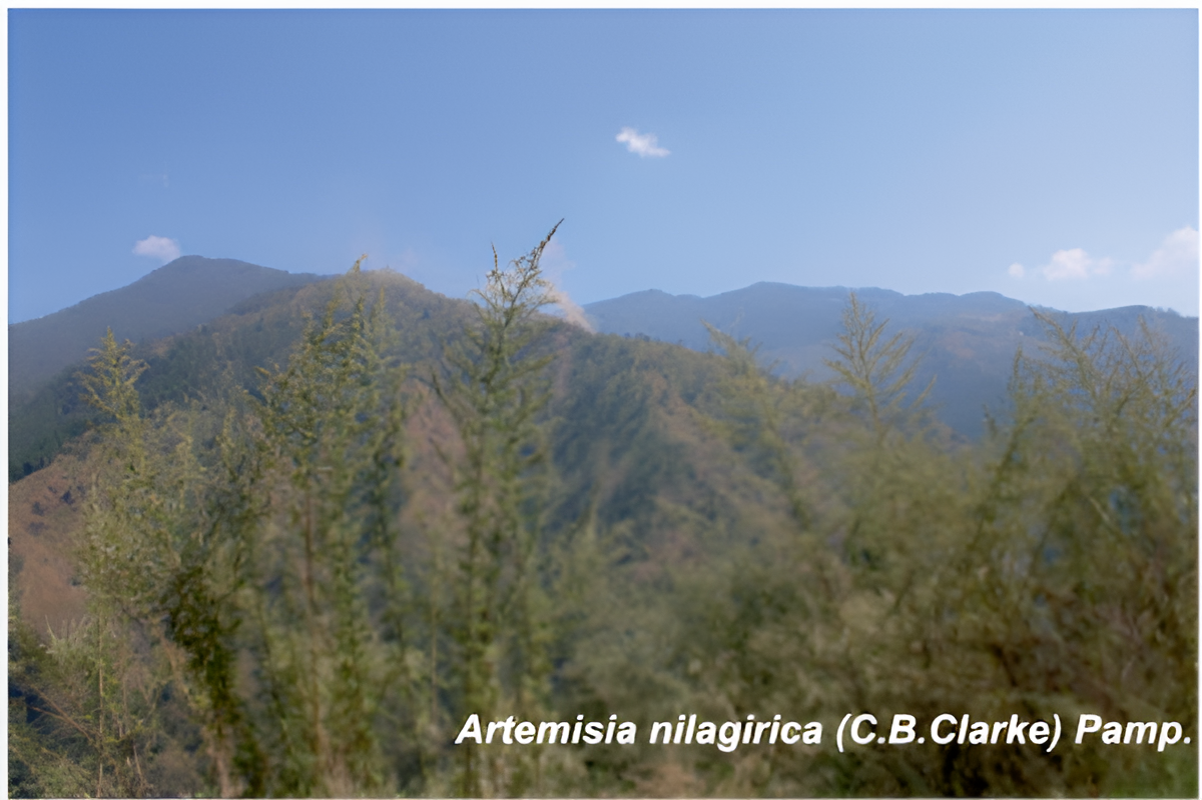
कालरात्रि देवी दुर्गा का सातवां स्वरूप हैं, जिन्हें नवरात्रि के सातवें दिन पूजा जाता है। वे अंधकार और बुराइयों का नाश करने वाली देवी हैं। देवी का यह स्वरूप नागदौन औषधि से संबंधित होता है।
- सम्बंधितपादप- नागदौन
- वैदिक नामःदेवाज्यकः पूतः
- वानस्पतिक नाम: Artemisia nilagirica (C.B.Clarke) Pamp.
- संस्कृत नामः इस पादप को संस्कृत में दमनकः, दान्तः, मुनिपुत्रः, तपोधनः, गन्धोत्कट, ब्रह्मजट, विनीत, कलपत्रक, दमन आदि नामों से जाना जाता है।
चिकित्सीय उपयोगः
नागदौन एक प्रभावी औषधि है, जो मस्तिष्क शक्ति बढ़ाने और तनाव, डिप्रेशन, ट्यूमर व अल्जाइमर से बचाव में सहायक है। दमन ककटु, तिक्त, कषाय, शीत, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, त्रिदोष शामक, हृद्य, वृष्य, सुगन्धित, ग्राही, स्तम्भक, बल कारक तथा रसायन होता है। यह विष, कुष्ठ, क्लेद, कण्डू, विस्फोट, आम दोष तथा भूतबाधा शामक होता है। इसके पत्र स्तम्भक, कटु, शोथहर, व्रण विरोहक, मूत्रल, आर्तवजनन, वाजीकारक, क्षुधावर्धक, पाचक, कृमिघ्न, ज्वरघ्न तथा रक्त वर्धक होते हैं। इसकी मूल बलकारक एवं पूयरोधी होती है। इसके पुष्प श्वास, कास, शोथ, कुष्ठ, त्वम्-रोग, मूत्र कृच्छ्र, शूल, आत्रकृमि, ज्वर तथा पाण्डु-शामक होते हैं।
8. अष्टमः नवदुर्गारूपः महागौरी-
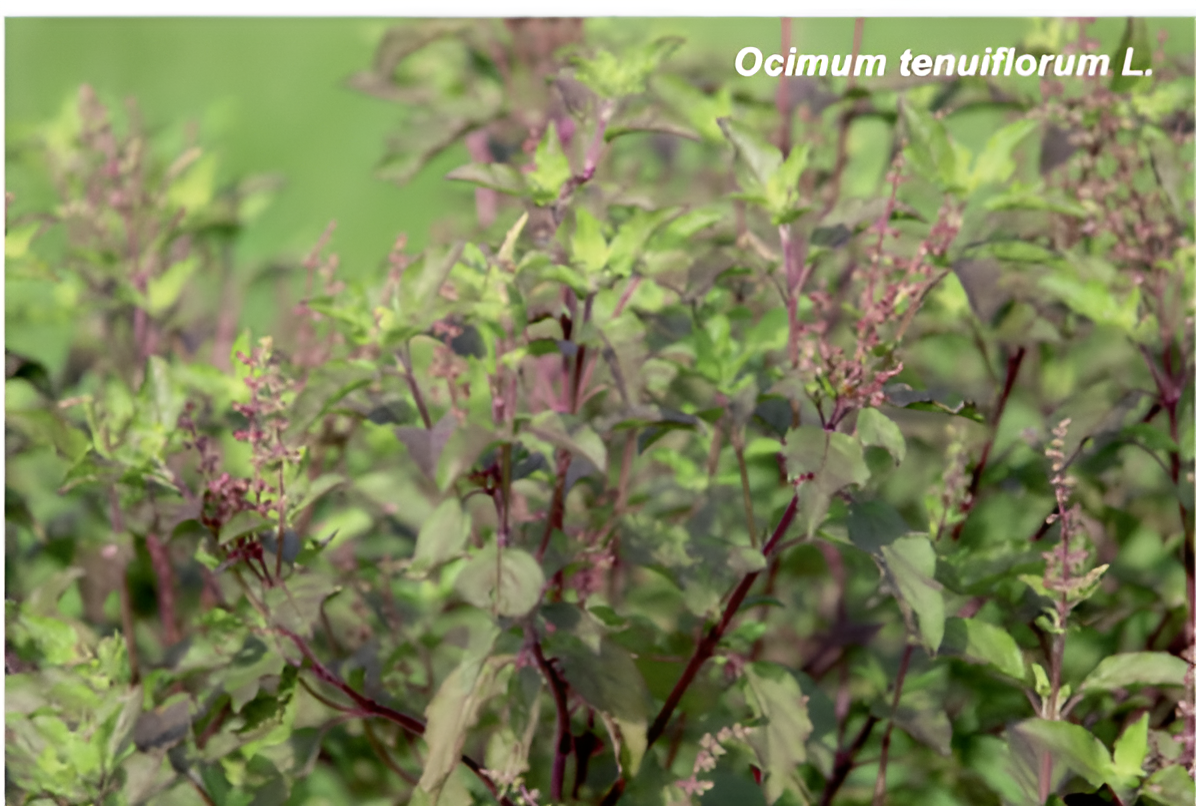
महागौरी, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। अष्टमी के दिन उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वे सौंदर्य, शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। देवी का यह स्वरूप तुलसी औषधि से संबंधित होता है।
- सम्बंधितपादप- तुलसी
- वैदिक नामः सुमज्ञ्जरिकारामा
- वानस्पतिक नाम: Ocimum tenuiflorumL.
- संस्कृत नामः इस पादप को संस्कृत में तुलसी, सुरसा, देवदुन्दुभिः, अपेतराक्षसी, सुलभा, बहुमञ्जरी, गौरी, भूतघ्नी; आदि नामों से जाना जाता है।
चिकित्सीय उपयोगः
सुखवल्लरी, श्री कृष्ण-बल्लभा, वृन्दा, वैष्णवी आदि पवित्र नामों से विभूषित तुलसी के माहात्म्य का वर्णन करना ऐसा है, जैसे सूरज को दीपक दिखाना, या समुद्र किनारे बैठकर लहरों को गिनना। सर्वरोग निवारक, जीवनीय-शक्तिवर्धक, इस औषधि को प्रत्यक्ष देवी कहा गया है; क्योंकि सर्वत्र सुलभ, सुगन्धित, सुन्दर तथा इससे उपयोगी औषधि मनुष्य जाति के लिए अन्य कोई और नहीं है। तुलसी के धार्मिक महत्व के कारण हर घर आगंन में इसके पौधे लगाए जाते हैं। तुलसी पञ्चाङग कफ वात शामक, जन्तुघ्न, दुर्गन्धनाशक, दीपन, पाचन, अनुलोमन, कृमिघ्न, कफप्घ्न, हृदयोत्तेजक, रक्तशोधक, स्वेदजनन, ज्वरघ्नव शोथहर होता है। तुलसी के बीज मूत्रल एवं बलकारक हैं। तुलसी के पत्र प्रतिश्याय, वातश्लैष्मिक ज्वर एवं विषम ज्वर में लाभप्रद है। तुलसी पञ्चाङगश्वास, श्वसनीशोथ, कर्कटार्बुद (बड़ीआंत, यकृत्, पित्ताशय), कवकरोग, हृदयविकार, प्रतिश्याय, विसूचिका, उदरशूल, विबन्ध, कास, ऐंठन, मानसिक अवसाद, त्वक्विकार, अतिसार, कष्टार्तव, अग्निमांद्य, श्वासकष्ट, कर्णशूल, मस्तिष्करोग, आंत्ररोग, नासास्राव, ई. कोलाईसंक्रमण, ज्वर, कवक संक्रमण, आमाशयिकरोग, सूजाक, अश्मरी, शिरोवेदना, पक्षाघात, यकृत्विकार, हिक्का, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, श्वित्र, कटिशूल, मलेरिया, अक्षिरोग, कर्णरोग, पूतिनासा, आमवात, दद्रु, सर्पदंश, प्लीहा रोग, शोथ, क्षय, व्रण, रतिजरोग, विषाणुसंक्रमण, अधिमांस एवं कृमि रोग में लाभप्रद होता है।
9. नवमः नवदुर्गारूपः सिद्धिदात्री-

दुर्गा का नौवां रूप सिद्धिदात्री हैं, जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन इनकी पूजा की जाती है। देवी का यह स्वरूप शतावरी औषधि से संबंधित होता है।
- सम्बंधितपादप- शतावरी
- वैदिक नामः शतावरकः अधरकण्टः
- वानस्पतिक नाम: Asparagus racemosus Willd.
- संस्कृत नामः इस पादप को संस्कृत में शतावरी, शतपदी, शतमूली, महाशीता, नारायणी, काञ्चनकारिणी, पीवरी, सूक्ष्मपत्रिका, अतिरसा, भीरु, नारायणी, बहुसुता, आदि नामों से जाना जाता है।
चिकित्सीय उपयोगः
भावप्रकाश निघण्टुकार के अनुसार यह गुरु, शीत, तिक्त, रसायन, बुद्धिवर्धक, अग्निवर्धक, वात, पित्त, शोक-
निवारक, शुक्र दुर्बलता को दूर करने वाली तथा स्तन्य-क्षय को दूर करने वाली है। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार शतावरी बुद्धिवर्धक एवं अग्नि वर्धक, बलकारक तथा दूषित-शुक्र का शोधन करती है। धन्वन्तरिनिघंटुकार के अनुसार शतावर जीर्ण से जीर्ण रोगी कोपुनः बल तथा रोग से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है- अर्थात्शरीर इसके सेवन से रोग निवारक क्षमता को पुनः प्राप्त करता है। यह वात पित्तशामक, शुक्रजनन, शीतल, मधुर तथा दिव्य रसायन है। आचार्य चरक ने शतावर को बलकारक, वयः स्थापक तथा मधुर बताया है। इसकी मूल शीतल, मूत्रल, पोषक, बलकारक, स्तन्यजनन, वाजीकर, विरेचक, कफनिःसारक, मृदुकारी, वयःस्थापक, वातानुलोमक, क्षुधावर्धक, आमाशय-रसवर्धक, आमातिसार तथा मधुमेह शामक होते हैं। इसके पत्र केश्य, स्तन्य जनन तथा हिक्का नाशक होते हैं।